भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों का भुला दिया गया इतिहास
(The forgotten history of Indian international relations)
Posted on February 7th, 2019 | Create PDF File
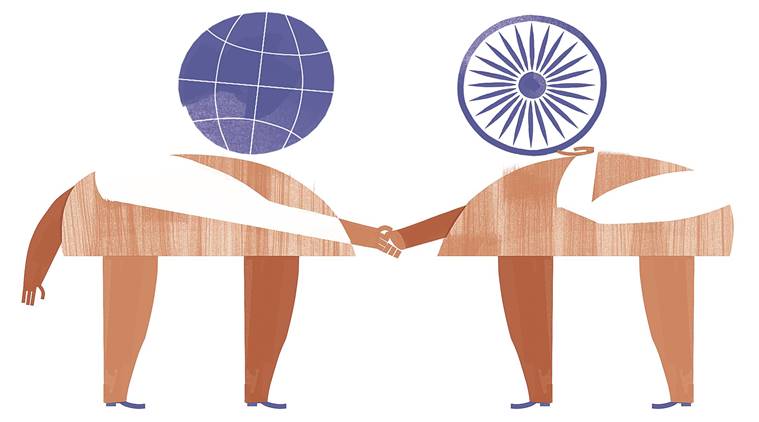
दक्षिण एशिया में अंतरराष्ट्रीय संबंधों (आईआर) की उत्पत्ति, उद्देश्य और मौजूदगी के भुला दिए गए इतिहास के पुनर्मूल्यांकन का समय आ गया है।
अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भारतीय दृष्टिकोण’ का क्या मतलब है? भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों (आईआर) को यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आम तौर पर पश्चिमी शिक्षण परंपरा से उपजा हुआ माना जाता है। यह विचार दक्षिण एशियाई बुद्धिजीवियों, विद्वानों और कार्यकर्ताओं के बीच 20वीं शताब्दी के दौरान उभरे राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय विचारों के व्यापक कार्य को व्यक्त नहीं करता। दक्षिण एशिया में आईआर की उत्पत्ति, उद्देश्य और मौजूदगी के भुला दिए गए इतिहास के पुनर्मूल्यांकन का समय आ गया है। इसमें वह शिक्षण परंपरा सामने आती है जो आईआर के दायरे को व्यापक करती है, और उपनिवेश के बरक्स उपनिवेश विरोधी शक्तिशाली वैश्विक दृष्टिकोण को सामने लाती है और स्वतंत्र भारतीय विदेश नीति की आधारशिला रखती है। समकालीन विद्वानों और भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए।
परिचय-
“भारत से बाहर का अकादमिक जगत वास्तव में भारतीय सामाजिक और राजनितिक संगठन की व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए व्यग्र है। राजनीति विज्ञान में शोध... तभी हकीकत बन सकेगा जब भारतीय विषयों में अध्ययन के लिए व्यापक प्रावधान किए जाएंगे।”
— एम. वेंकटरंगैया, ‘कोर्सेज ऑफ स्टडीज इन पोलिटिकल साइंसेज’, 1944
अंतरराष्ट्रीय मामलों की भारतीय अवधारणा की संभावना अक्सर एक विवादित और बेहद राजनीतिक बहस को पेश करती है। इसमें हैरानी नहीं कि यह चर्चा अक्सर भारत की बेहतर होती स्थिति, चीन और दूसरी जगहों पर हो रहे विकास और सामाजिक विज्ञान के व्यापक उद्देश्य और स्वायत्तता के गूढ़ सवालों के संदर्भ में होती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों (आईआर) को भारतीय देन के बारे में जानने की इच्छा इस संबंध में हो रही व्यापक चर्चा से पहले शुरू हो गई थी जो दक्षिण एशियाई विद्वान अमिताव आचार्य की ओर से 2014 के इंटरनेशनल स्टडीज एसोसिएशन में किए गए अध्यक्षीय संबोधन के दौरान ‘ग्लोबल आईआर’ की जरूरत को ले कर उठाए गए सवाल से तेज हुई है। आचार्य ने ग्लोबल आईआर को ले कर जो धारणा पेश की है वो हाल के दशकों में दुनिया भर में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए इंटरनेशल रिलेशंस विभागों के साथ जुड़ने की वकालत करती है। ताकि इस क्षेत्र का दायरा व्यापक हो, क्षेत्रीयतावाद को ले कर नए विचार सामने आएं और सैद्धांतिक परंपरा की महत्वपूर्ण स्थिति की पुनर्संरचना को बढ़ावा मिले।
अंतरराष्ट्रीय मामलों की भारतीय अवधारणा की संभावना अक्सर एक विवादित और बेहद राजनीतिक बहस को पेश करती है। इसमें हैरानी नहीं कि यह चर्चा अक्सर भारत की बेहतर होती स्थिति, चीन और दूसरी जगहों पर हो रहे विकास और सामाजिक विज्ञान के व्यापक उद्देश्य और स्वायत्तता के गूढ़ सवालों के संदर्भ में होती है।
अंतरराष्ट्रीय संबंध के विषय को ‘वैश्विक बनाने’ की कोशिश का बहुतों ने स्वागत किया है। इसके बावजूद जैसा कि आचार्य की टिप्पणी संकेत करती है कि इस बहस के बीच भारत और दूसरी जगहों पर अंतरराष्ट्रीय विचार के विकास का इतिहास विराजमान है। ‘ग्लोबल आईआर’ की वकालत करने वालों और दक्षिण एशियाई अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के बहुत से तरफदारों की यह आदत रही है कि भारतीय आईआर को सिर्फ ‘विकसित हो रहे’ की स्थिति में पेश करें। भारतीय आईआर की ‘अनुपस्थिति’ को ले कर बहुत मजबूत कथ्य मौजूद रहा है और यह हाल संयुक्त राज्य में रह रहे दक्षिण एशियाई विद्वानों का भी रहा है।जहां नेहरू, टैगोर और गांधी जैसी शख्सियतों को दक्षिण एशियाई अंतरराष्ट्रीय विचार के एक समूह के तौर पर पर्याप्त ध्यान मिला, लेकिन 1947 से पहले इस विषय को अस्तित्व विहीन मान लिया गया था। कुछ साहसी अपवाद जरूर रहे हैं, लेकिन बहुतों के लिए भारतीय आईआर पश्चिमी आईआर के प्रतिमानों और सिद्धांतों — रचनात्मकतावाद, वास्तविकतावाद, उदारवाद पर सवार मान लिया गया है, जिसमें संभवतः उत्तर औपनिवेशिक स्थिति के लिए बहुत संकीर्ण स्थिति है।
इस इतिहास की समीक्षा की जरूरत है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान के विषयों में भारतीय विद्वान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर औपनिवशिक दृष्टिकोण को ले कर बहुत मुखर थे और काफी प्रयासरत थे। यह सिर्फ एक विद्वतापूर्ण प्रयास ही नहीं था। अंतरराष्ट्रीयवाद के विचार के बौद्धिक बीज युद्धों के बीच के काल में लगातार पनपते गए। इसमें पहले विश्व युद्ध की बर्बरता का असर था और उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता आंदोलनों का प्रभाव था। इसमें राष्ट्रवादी परियोजनाएं भी शामिल थीं, हालांकि यह इस तक ही सीमित नहीं था। विविध राजनीतिक और बौद्धिक क्षेत्र पर जमे हुए यह लेखागार इंडियन पोलिटिकल साइंस एसोसिएशन जैसे शुरुआती भारतीय विद्वत सोसाइटियों, उत्तर अमेरिका में स्थित प्रवासी समुदाय के पंफलेट और न्यूजलेटर और बौद्धिक आदान-प्रदान के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, जिनमें दक्षिण भारतीय विद्वान शामिल थे, तक में शामिल थे। यह व्यापक बौद्धिक आदान-प्रदान आज भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक गहरा और ज्यादातर भुला दिया गया इतिहास और भारतीय अंतरराष्ट्रीय विचार, सिद्धांत और अनुभव पेश करता है।
आधुनिक आईआर विचार: भारत के अग्रदूत-
भारत में आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विचार के शुरुआती प्रमुख व्यक्तियों में एक थे बंगाली समाजशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतकार बिनोय कुमार सरकार। उन्होंने विभिन्न प्रकाशनों में अपनी जगह बनाई जिनमें अमेरिकन पोलिटिकल साइंस रिव्यू, पोलिटिकल स्टडीज क्वाटरली और जर्नल ऑफ रेस डेवलपमेंट (बाद में जो फॉरन अफेयर्स बन गया) जैसे प्रमुख अमेरिकी राजनीति विज्ञान प्रकाशन भी शामिल हैं। सरकार के काम ने दक्षिण एशियाई बुद्धिजीववाद को अमेरिका और यूरोप के शुरुआती दौर के राजनीति विज्ञान के साथ एकाकार कर दिया। एपीएसआर में 1919 में प्रकाशित उनके लेख ‘हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस’ में कौटिल्य और कमंडकिय नीतिसार की शिक्षाओं को मंडल (जिसे बाद में नेहरू ने ज्यादा विस्तार से बताया) के सिद्धांतों के साथ मिश्रित किया गया था। इसे उन्होंने “हिंदू आइडिया ऑफ बैलेंस ऑफ पावर” बताया। वैदिक ग्रंथों को पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय विचारों के संदर्भ में देखने की यह इच्छा सर्वभौम के विश्लेषण में भी सामने आई। यह ‘स्थायी शांति’ और औपनिवेशिक संघ तथा लीग ऑफ नेशंस के समकालीन विचार का हिंदू समकक्ष था।
सरकार के काम में पश्चिमी विचारों का जम कर संदर्भ दिया गया था, जिनका अनुभव उन्होंने संयुक्त राज्य और यूरोप में बिताए अपने समय के दौरान किया था। लेकिन उनकी विद्वता सिर्फ अनुकरण करने की सामान्य प्रक्रिया तक सीमित नहीं थी। यात्राओं के दौरान उन्हें जो वैश्विक बौद्धिक अनुभव हुए थे, उनके आधार पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मामलों के पश्चिमी ज्ञान को एक गंभीर चुनौती दी। उदाहरण के तौर पर 1919 के उनके लेख, ‘फ्यूचरिज्म ऑफ यंग एशिया’ ने उन ‘पश्चिमी तर्कों की आलोचना’ शुरू कर दी जिनमें पूर्व की ऐतिहासिक उपलब्धियों को लगातार नकारा जाता रहा है। उन्होंने इसे पूर्ववाद का नाम दिया और एडवर्ड सईद के उत्तर उपनिवेशाद के कई दशक पहले ही इसे अंकित कर दिया। यह वाद व्यवस्थित तौर पर पूर्व को बदनाम कर रहा था और इसे ठहराव और अध्यात्म का ठिकाना बताता था। इसकी बजाय सरकार ने तर्क पर जोर दिया और दिखाया कि यूरोपी अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय गर्व की अव्यवहारिक मान्यता पर टिकी हुई है, एक खास तरह का आदर्शवाद जो युगोस्लाविया, चेकोस्लाविया और पोलेंड की बहुनस्लीय विशिष्टता पर टिका था।पोलिटिक्स ऑफ बाउंड्रीज एंड टेंडेंसीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस (1926) में, जो संभवतः अंतरराष्ट्रीय मामलों पर उनका सबसे व्यवस्थित अध्ययन था, उन्होंने ‘राष्ट्रीयता के सिद्धांत से मुक्ति... राष्ट्रभक्तों और आदर्शवादियों की ओर से थोपे गए रहस्यमयी संबंध... एक पंथ के तौर पर राष्ट्रीयता के रोमांचक विचार’ को चुनौती दी।संक्षेप में, यह पश्चिमी ज्ञान का उसी के खिलाफ उपयोग करने का एक प्रयास था; प्रति ज्ञान का एक स्वरूप जो एक साथ दक्षिण एशियाई पहचान को भी हासिल करता था और बौद्धिक स्पंदन को भी। इस दौरान यह पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय विचार के अंतर्विरोध को भी प्रदर्शित करता था। ‘उपनिवेशों’ में भरे जा रहे मेट्रोपिलटन अंतरराष्ट्रीय विचार का वाहक बनने की बजाय सरकार ने साहसी बौद्धिक आलोचना में योगदान किया। इस बीच यूरोप में पहले विश्व युद्ध के खंडहरों से एक नया समाज विज्ञान उभर रहा था। गैर-पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय विचार में यह एक अहम योगदान था, जो ई.एच कार, नोर्मन एंजेल जैसों और प्रथम विश्व युद्ध उपरांत के बनाए गए एबरविस्टविथ यूनिवर्सिटी और वेल्स के वूड्रॉव विल्सन पीठ (जिसे महा युद्ध के डर से बचाने के लिए तैयार किया गया था) के प्रपंच में पूरी तरह डूब गया था।
सरकार के काम में पश्चिमी विचारों का जम कर संदर्भ दिया गया था, जिनका अनुभव उन्होंने संयुक्त राज्य और यूरोप में बिताए अपने समय के दौरान किया था। लेकिन उनकी विद्वता सिर्फ अनुकरण करने की सामान्य प्रक्रिया तक सीमित नहीं थी।
इस परियोजना में सरकार अकेले नहीं थे। पहले विश्व युद्ध के खौफनाक मंजर के दौरान जर्नल ऑफ रेस डेवलपमेंट में एम. एन. चटर्जी ने अपने लेख के जरिए भविष्य में नस्लीय आधार पर होने वाले वैश्विक संघर्ष की झलक दे दी। इसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उपनिवेशवादी ताकतों की ओर से अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने में नाकामी एक संघर्ष की ओर ले जाएगी। जैसा कि सेमिल आडिन ने बताया है, यह उस समय पूरे एशिया में चल रहे व्यापक पश्चिम विरोधी बौद्धिक आंदोलन को ही प्रदर्शित कर रहा था।चटर्जी की भविष्यवाणी पश्चमी सभ्यता के द्वंद और पाखंड पर आधारित थी जो पूर्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाने की बात करती थी, जबकि उसी दौरान यूरोप में एक-दूसरे को नष्ट करने के बर्बर युद्ध में जुटी हुई थी। यह ऐसा युद्ध था जो उच्च वर्ग की ओर से निम्न वर्ग के शोषण पर आधारित था और जो नोर्मन एंजेल, विक्टर ह्यूगो, जॉन ब्राइट और शांति अध्ययन की पूरी पश्चिमी बटालियन का मजाक बना रहा था।
20वीं शताब्दी के समाज विज्ञान की पश्चिम केंद्रित आलोचना बहुत व्यापक थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के वी.एस. राम और पी.एन. मसलदान भी यूरोपीय ‘शांति के सिद्धांत’ के उतने ही कटु आलोचक थे। इनका आधार था कि “यह एक अनैतिक मान्यता है कि विश्व का एक हिस्सा लंबे समय तक साम्राज्यों का उपनिवेश बना रहेगा और उन्हें पश्चिमी कूटनीति के खेल में महज प्यादे के तौर पर माना जाएगा।” उन्होंने तर्क दिया, “शांति के बारे में शुद्ध रूप से यूरोपीय दृष्टिकोण से देखा जाए” तो मौलिक सत्यता यही निकलेगी कि औपनिवेशिक इच्छाओं से ही युद्ध और संघर्ष निकले हैं।उनके सहकर्मी बी.एम. शर्मा जो उसी विश्वविद्यालय के थे, उन्होंने भी ‘यूरोपीय शांति का मतलब विश्व की वास्तविक सुरक्षा है’ की भ्रांति पर उतना ही जोरदार हमला किया। उन्होंने अंग्रेजी सिद्धांतकारों और खास तौर पर लंदन स्कूल ऑफ इकनोमिक्स के लेक्चरर हैरोल्ड लास्की के मार्क्सवाद प्रभावित विचारों और पत्रकार क्लारेंस स्ट्रेट के लोकतांत्रिक संघवाद का जम कर जवाब दिया।
यह आगे चल कर विश्व व्यवस्था के यूरोपीय विचार का औपनिवेशीकरण में बदल गया जहां नए विचार पेश करने वाले भी समन्यव पर जोर देने लगे और दक्षिण एशियाई बुद्धिजीवी परंपरा को यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी के साथ एकसार कर दिया गया। कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज के बी.एम. शर्मा और देव राज के काम इसके खास उदाहरण हैं।अंतरराष्ट्रीय मामलों में नैतिक बल और अहिंसा के गांधीवादी विचार को युद्धों के बीच महाशक्ति प्रबंधन के विचार और संस्थाओं के नाकाम उपनिवेश और साम्राज्यवादी नियंत्रण की समाप्ति के साधन के तौर पर पेश किया गया। इसके बावजूद यह ई. एच कार के ट्वेंटी ईयर्स क्राइसिस, विल्सोनियन अंतरराष्ट्रीयवाद के विचार और एच.जी. वेल्स के राजनितिक लेखों के पाठ के साथ-साथ चलता रहा। संक्षेप में, इन अग्रदूतों ने अंतरराष्ट्रीय के विकेंद्रित दृष्टिकोण को पेश किया, जिसमें हमें इतिहास और अंतरारष्ट्रीय मामलों के यूरोपीय दृष्टिकोण पर आधारित एक मूल कहानी से साथ संवाद करते हुए उससे दूर ले जाया गया।
परियोजनाएं-
20वीं शताब्दी के शुरुआत के भारतीय अंतरराष्ट्रीय विचार के अग्रदूत इस तरह अपने साथ विश्व स्तर पर उपनिवेशवाद विरोधी और स्वतंत्रता आधारित विचार ले कर चल रहे थे। अपने विद्वतापूर्ण प्रयासों के साथ ही उनमें से कई के ऐसे राजनीतिक संगठनों से भी संबंध थे जो औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के लिए कार्यरत थे। उदाहरण के तौर पर, राजनीतिक वैज्ञानिक तारकनाथ दास जहां संयुक्त राज्य में कामयाब अकादमिक कैरियर को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे थे और स्कूल ऑफ फॉरन सर्विस व जोर्जटाउन विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे थे और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय दोनों जगह लेक्चर दे रहे थे, वहीं वेस्ट कोस्ट से चल रहे उपनिवेश विरोधी गदर आंदोलन में भी साथ थे। दास को बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन अनुशीलन समिति में बचपन में ही शामिल कर लिया गया था। बाद में उन्होंने बिनोय कुमार सरकार, जिनके भाई धीरेन सरकार भी गदर के प्रमुख सदस्य थे, को भी इसमें शामिल किया। उनकी पत्नी मैरी कीटिंग मोर्स अमेरिका से चलने वाले नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल की सह-संस्थापक थी। सरकार के पूर्व छात्र एम.एन. रॉय (जिन्हें नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है) आगे चल कर 1920 के दशक के दौरान प्रसिद्ध कार्यकर्ता बने और लेनिन के वार्ताकार भी, जिन्होंने मैक्सिको के आंदोलनकारियों के साथ समय बिताया।
ये सभी राजनीतिक गतिविधियां अपने स्वरूप में विद्रोही नहीं थीं। शुरुआती भारतीय राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को राष्ट्रवाद की परियोजना से पूरी तरह जोड़ कर देखना भी गलत होगा। इसके बावजूद उनके काम और गतिविधियों में राष्ट्र निर्माण का मजबूत प्रवाह बना रहा। इस लिहाज से ये भारत में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन की नीव रखने वाले साबित हुए। 1938 में स्थापित इंडियन पोलिटिकल साइंस एसोसिएशन (आईपीएसए) और इसके प्रकाशन इंडियन जर्नल ऑफ पोलिटिकल साइंस ने भारतीय विद्वानों को राजनीतिक सिद्धांत, संविधानवाद और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर लिखने का मंच प्रदान किया। भारत भर के विश्वविद्यालयों से इसके सदस्य शामिल किए गए, जिनमें बी.के. सरकार, पी.एन. सप्रू और ए. अप्पादुरई जैसे प्रख्यात लोग भी शामिल थे। आईपीएसए का पहला सम्मेलन वाराणसी में 1939 में आयोजित किया गया और इसमें ‘नेचर ऑफ सोवर्नटी’, ‘इंडियंस इन सीलोन’ और ‘ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस थ्रू टेक्निकल कॉपरेशन बिटविन नेशंस’ जैसे विषय शामिल थे। उस समय की युनाइटेड प्रोविंस के प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने भारत में स्वतंत्रतामूलक राजनीतिक विज्ञान का नैतिक उद्देश्य से उपयोग करते हुए भारत के आत्मबोध में इस्तेमाल पर भाषण दिया जो स्पष्ट तौर पर स्वतंत्रता और स्वराज के लिए राष्ट्रीय परियोजना थी।
आईपीएसए ने भारत में नए विषय राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन को एक मंच दिया। आईपीएसए सदस्य अप्पादुरई, सप्रू और हृदय नाथ कुंजरू ने आगे चल कर 1955 में दिल्ली विश्वविद्यालय में इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (जो बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चला गया) और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्लूए) की स्थापना की। आईसीडब्लूए भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मामलों का स्वतंत्र थिंक टैंक था। अकादमिक जगत, सरकार और सिविल सोसाइटी तक के लोग इसके सदस्य बने और आईसीडब्लूए ने ऐसा “गैर सरकारी और गैर राजनीतिक संगठन उपलब्ध करवाया जहां भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके।”आईसीडब्लूए जैसे संस्थान ही थे, जहां भारत में राजनीति विज्ञान के शुरुआती आंदोलन के विद्वता भरे काम को जगह मिली और तत्कालीन नीतिगत चर्चाओं में इसकी आवाज सुनी गई। इसके बावजूद यह आंदोलन अब तक असमान और अपूर्ण था। वी.के.एन. मेनन और ए. अप्पादुरई जैसे कुछ लोग तो इस विभाजन को दूर कर आईपीएसए और आईसीडब्लूए के प्रकाशन इंडिया क्वाटरली के लिए अपना सहयोग करते रहे, जबकि कुछ पूरी तरह से शोधपरक कार्यों में लगे रहे।
आईपीएसए ने भारत में नए विषय राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन को एक मंच दिया। आईपीएसए सदस्य अप्पादुरई, सप्रू और हृदय नाथ कुंजरू ने आगे चल कर 1955 में दिल्ली विश्वविद्यालय में इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (जो बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चला गया) और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्लूए) की स्थापना की। आईसीडब्लूए भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मामलों का स्वतंत्र थिंक टैंक था।
इसके बावजूद इंडिया क्वाटरली जिस तरह के विषयों पर जोर देता था, उसे देखते हुए यह साफ हो जाता है कि यह शुरुआती भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों के व्यवहारिक पक्ष को उभारने पर जोर दे रहा था। आईसीडब्लूए को अक्सर उस दौरान के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में ओब्जर्वर का दर्जा मिलता था। इस बारे में इंडिया क्वाटरली के इंडिया एंड वर्ल्ड खंड में व्यवस्थित तौर पर उल्लेख मिलता है। इनमें ब्रेटन वूड्स सम्मेलन (जहां इंटरनेशनल मोनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना की नीव पड़ी) और डोंबार्टन ओक्स भी शामिल है। डोंबार्टन ओक्स में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की व्यवस्था पर सहमति बनी। भारतीय प्रतिनिधि इन सम्मेलनों में स्वतंत्रता से पूर्व आवाज उठाने की कोशिश तो बहुत करते थे, लेकिन उनकी बात ज्यादा सुनी नहीं जाती थी, जो उस दौरान के शैशवकालीन कूटनीतिक दस्ते की चिंता को भी जाहिर करता है। इन चिंताओं में हिंसक नागरिक युद्ध और उपनिवेश विरोधी संघर्ष वाली क्षेत्रीय शक्तियों जैसे बर्मा, इंडोनेशिया और चीन को मान्यता मिलना भी शामिल था। लेकिन ज्यादा बड़ी कूटनीतिक चिंता भारतीय प्रवासियों के दर्जे को ले कर थी जो पतन की ओर बढ़ रहे ब्रिटिश सम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में बसे थे। इंडिया क्वाटरली के सहायक संपादक सी. कोंडपी ने नियमित कॉलम ‘इंडियन ओवरसीज’ में बर्मा, मलाया, सिलोन, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और अन्य देशों के प्रवासियों के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा था, “भारतीयों, स्थानीय लोगों और यूरोपीय समुदायों के बीच आर्थिक मुकाबले और नस्लीय तुलना की वजह से और एक छोटे नस्लीय अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीतिक प्रभुत्व की वजह से उनके नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर बहुत तरह की पाबंदियां लगी थीं। इनमें अंतिम संस्कार से ले कर संसदीय प्रतिनिधित्व तक शामिल हैं।” इस विवादित नीतिगत मुद्दे के बीच ही विभिन्न देशों में फैले भारतीय समुदाय का उदय हुआ, व्यापक भारत की परिकल्पना सामने आती दिखने लगी जो औपनिवेशिक राज के अन्याय और इसके नस्लीय, कानूनी और राजनीतिक भेद-भाव पर सवाल उठा रही थी।
निष्कर्ष-
जैसा कि इस आलेख के शुरुआती उद्धरण में कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में भारतीय आयाम की खोज नई नहीं है। अंतरराष्ट्रीय विचार के इतिहास और भारत में राजनीतिक विज्ञान के उदय पर गौर करें तो भारतीय राष्ट्र के इतिहास में अंतरराष्ट्रीय मामलों पर दक्षिण एशियाई नजरिए को आगे बढ़ाने के भारतीय विद्वानों के लगातार होते रहे प्रयासों का पता चलता है। इतिहास बताता है कि शक्ति के लिए हुए महायुद्ध की रक्षा का इस विषय की परिभाषा पर ना तो एकाधिकार था और ना है। अंतरराष्ट्रीय विचार यूरोप और उत्तरी अमेरिका का विशेषाधिकार नहीं था। बल्कि यह विभिन्न स्थानों से वैश्विक संवाद के तौर पर उभरा। इसमें सम्राज्य के हित और अनुभव, उपनिवेश विरोध, राष्ट्रीय आंदोलन और वैश्विक बौद्धिक नेटवर्क सभी शामिल थे। भारतीय विद्वानों ने अंतरराष्ट्रीय विचार को समझने और दर्ज करने के इस दुबारा मजबूत हुए प्रयास में एक सक्रिय भूमिका निभाई और इस विषय के बारे में एक नया नजरिया पेश किया, जिसमें नस्ल, उपनिवेश विरोधी, अंतरराष्ट्रीय एकजुटता और उत्तर औपनिवेशिक विश्व व्यवस्था के लिए पुनर्कल्पित दृष्टिकोण जैसे विषय शामिल थे।
जहां जाहिर तौर पर मौजूदा विश्व परिदृष्य की राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका के संदर्भ में दक्षिण एशियाई अंतरराष्ट्रीयवाद के दृष्टिकोण को फिर से तलाशने में दिलचस्पी होगी लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए ऐसे अंतरराष्ट्रीय विचार को फिर से तलाशना कुछ मायनों में ऐसे अध्ययन के लाभ को कम कर सकता है। अपनी राजनीतिक और बौद्धिक स्थिति से इतर, इन बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय विचारों के वैश्विक आदान-प्रदान में वाहक की भूमिका निभाई। चीन, जापान और पूर्वी एशिया से ले कर यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक फैले विद्वत नेटवर्क से जुड़े होने की वजह से वे ना सिर्फ भविष्य की विश्व व्यवस्था के दक्षिण एशिया के दृष्टिकोण के दूत के तौर पर बल्कि भारत में चल रहे राजनीतिक बदलाव को पेश करने वालों के तौर पर भी सामने आए। इसके बावजूद यह महत्वपूर्ण है कि इन पाठों को जो उन्हें विशिष्ट तौर पर भारतीय के तौर पर पेश करते हैं या जो उन्हें गैर-पश्चिमी समाज विज्ञान के असली उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं, उन्हें सतर्कता से लिया जाए। ऐसे पुरालेख को मिलने वाली अहमियत का मूल्य विश्व व्यवस्था की वैकल्पिक जड़ों को प्रकट करने की क्षमता में है, जो उस समय के अंतरराष्ट्रीय बदलाव में मौजूद थी। यह वैश्विक बौद्धिक संवाद की प्रक्रिया थी जो शायद एक असमान संवाद था। लेकिन इसी ने उत्तर औपनिवेशिक दक्षिण एशियाई अंतरराष्ट्रीयवाद का आधार खड़ा किया। जैसे भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध का अधिकांश हिस्सा उपनिवेश के खिलाफ उभरा, वैसे ही पश्चिमी आईआर गैर-पश्चिम राजनीतिक मुक्ति की पृष्ठभूमि में मजबूत हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि पश्चिमी आईआर ने भारतीय आईआर को इस तरह अपनी छाया में कैसे ले लिया। यह पुरालेख उन लोगों को मौका देता है जो दक्षिण एशियाई अंतरराष्ट्रीय संबंध की जड़ों को समझना चाहते हैं और साथ ही यह उन लोगों को सावधान करने की कोशिश भी है जो मानते हैं कि आईआर ऐसा विषय है जिसे पूरी तरह पश्चिम ने ही तैयार किया है। यह एक वैश्विक संवाद था और वैश्विक आईआर ही इसके नतीजों को पूरा कर सकता है।
विश्व परिदृष्य में भारत के भविष्य को ले कर 20वीं शताब्दी की शुरुआत और स्वतंत्रता उपरांत के शुरुआती दिनों के बहुत से दक्षिण एशियाई विद्वानों के अपने अंतर्निहित और सुस्पष्ट मत थे, उनकी विद्वता संकेत करती है कि संभवतः इसमें कुछ खो गया। 1950 के दशक के नेहरूवादी सुधार ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय अध्ययन को एक राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर बदल दिया जो एक उपयोगी ज्ञान का स्वरूप था। इसके बाद के काल में इसने इस विषय की राजनीतिक स्वायत्तता को काफी नुकसान पहुंचाया। स्वतंत्रता उपरांत राज्यों के साथ संबंधों पर जोर, शीत युद्ध शैली के क्षेत्रीय अध्ययन को अपनाना, सैद्धांतीकरण से बचाव या मैथडोलॉजिकल बहस, और संभवतः भारत के अपने अंतरराष्ट्रीय इतिहास के शोध में आई बाधा भी भारतीय आईआर के पतन की कहानी का हिस्सा रही हैं। भारतीय आईआर के इन अग्रदूतों के ब्योरे मिलें तो इस बड़ी खाई को कुछ पाटा जा सकता है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध का इतिहास अनुपस्थित नहीं है, बस इसे भुला दिया गया है।





